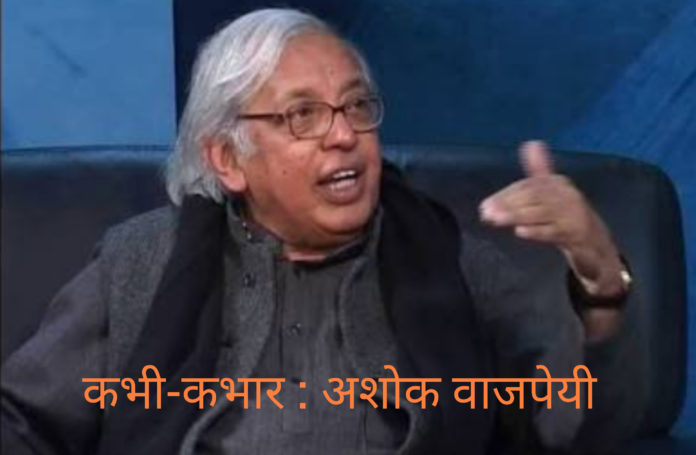हमारा लोकतंत्र एक गतिशील पर विचारशून्य व्यवस्था में तेज़ी से बदल रहा है
इन दिनों ज़रूरतों और उनको पूरा करने के तरीकों और साधनों पर बहुत ध्यान दिया जाता है. बहुत सारी ज़रूरतें दरअसल होती नहीं हैं, गढ़ी जाती हैं. विज्ञापन, कमतरी का अहसास, स्पर्धाभाव आदि ऐसी ज़रूरतें गढ़ते हैं. सारी बाज़ार-व्यवस्था, जिसका इन दिनों विचार से लेकर व्यवहार तक, धर्म से लेकर राजनीति तक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर अर्थव्यवस्था तक अभूतपूर्व बोलबाला है, मुख्यतः ज़रूरतें बनाने और पूरा करने पर आधारित है. हमारे नित फैलते मध्यवर्ग में ऐसे करोड़ों हैं और उनमें से अधिकांश युवा हैं, जिनका काम जूतों, माल की चमक-दमक, फ़ास्ट फूड, फिल्मों, पीठ पर बैग के बिना नहीं चलता पर पुस्तकों के बिना चल जाता है. उन पुस्तकों के जिन्हें पाठ्यक्रम में पढ़ना अनिवार्य होता है, उनमें भी अधिकांश का काम मूल पुस्तक से नहीं कुंजी से या गूगल से चल जाता है. ऐसे लोग असंख्य हैं जो रोज़मर्रा के व्यवहार में ज़रूरी प्रश्न, ‘क्या दाम है, कितनी दूर है, कौन आ रहा है’ आदि पूछे बिना तो नहीं चलते, पर ऐसे प्रश्न जीवन भर कभी न पूछे बिना जैसे ‘हम कौन हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमें कौन कहां ले जा रहा है, जीवन का अर्थ क्या है, दूसरे क्यों ज़रूरी है’ उनका काम बखूबी चल जाता है. अच्छा-ख़ासा जीवन बिताने और सभ्य-समृद्ध होने-कहलाने के लिए बहुत सारी मौलिक जिज्ञासा ज़रूरी नहीं होती. बहुतों को जीवन की आपाधापी में ऐसे प्रश्न पूछने की फुरसत ही नहीं मिलती.
हर समाज में भले प्रश्न पूछने, जिज्ञासा करने और विकल्प तलाशने का अधिकार और अवसर हर किसी का है, यह काम थोड़े से लोग ही करते हैं. यह थोड़ासापन उन्हें अकसर हाशिये पर ही रखता है. वे सब कुछ हाशिये से ही देखते-समझते-कहते हैं. ज़्यादातर लोगों का उन पर ध्यान भी नहीं जाता. यह एक तरह का श्रम-विभाजन है. वैचारिक-बौद्धिक-सर्जनात्मक श्रम कुछ लोग ही करते है. दूसरे जब-तब, ज़रूरत पड़ने पर, उनके किये-धरे का इस्तेमाल कर लेते हैं. यह बाज़ार में जाकर दिलो-जां ख़रीदने जैसा है जैसा कि ग़ालिब ने संकेत किया था.
कभी-कभी मन बहलाने के लिए, अपने अकेलेपन को भूलने के लिए लोगों को मुख्यतः मनोरंजन के लिए कुछ और की ज़रूरत लगती है. यह ‘कुछ और’ विचार, साहित्य, कलाएं आदि हैं. उनकी कभी-कभार की दरकार हाशिये पर ही रहती है.
कम से कम भारत में जैसा सांस्कृतिक रूप से निरक्षर या अल्पशिक्षित मध्यवर्ग विकसित हुआ और अपनी धाक जमाए हुए है, उससे लगता है कि अब उसे सृजन और विचार, जिज्ञासा और प्रश्नानकुलता की कोई ज़रूरत नहीं रह गयी है.
वह बने-बनाये उत्तरों से ज़रूरत पड़ने पर, जो कम ही जान पड़ती है, संतुष्ट हो जाता है. उसे भाषा नहीं जुमलेबाज़ी, संवाद नहीं झगड़े, आस्वाद नहीं मनोरंजन आदि रिझाते हैं. वह अकसर ईलियट के शब्दों में ‘आत्म-तुष्टि के सूअरबाड़े’ में महदूद रहकर अपने नागरिक होने की कृतार्थता समझता है. लोकतंत्र की एक बड़ी चूक या कमी यह है कि वह हर नागरिक को राजनैतिक तो बनाता है, विचारशील और प्रश्नवाची नहीं. जो हालत है उसमें, लगता है, तीख़े-जलते प्रश्न सिर्फ़ साहित्य और विचार में, कलाओं में पूछे जा रहे हैं और व्यापक लोकतांत्रिक समाज में, यह विडंबना है, वे प्रायः अनसुने हैं. हमारा लोकतंत्र एक गतिशील पर विचारशून्य व्यवस्था में तेज़ी से बदल रहा है.
कविता और चित्र
ऐसे कवि हैं जो चित्रकला के भी विशेषज्ञ हैं. फ्रांस में तो कलालोचना की शुरूआत ही एक महाकवि ने की और आज तक कवियों द्वारा कला की आलोचना उसका एक मूल्यवान अंग है. फ्रेंच कवि एपोलोनिएर ने कुछ चित्रकविताएं भी लिखीं हैं जिनमें कविता चित्र की तरह लिखी-आंकी गयी है. हिंदी में कलालोचना का एक बड़ा हिस्सा कवियों द्वारा लिखा गया है, जैसे कि अंग्रेज़ी में लिखी गयी भारतीय कलालोचना में कवि अग्रगामी रहे हैं. हमारे यहां महादेवी और शमशेर ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कविता लिखने के साथ-साथ चित्र भी बनाए हैं. शमशेर ने तो पिकासो आदि चित्रकारों पर कविताएं भी लिखी हैंं.
जान एशबरी एक अमरीकी मूर्धन्य कवि और अनुवादक होने के साथ-साथ चित्रकार भी थे. उन की कविताओं और कोलाजों का एक संचयन’ ‘दे न्यू वाट दे वाटेंड’ नाम से रिज़ाली इलेक्ता ने, मार्क पोली ज़ात्ती के संपादन में प्रकाशित किया है. इस संचयन पर दस वर्ष काम चला और स्वयं कवि ने उसका हर स्तर पर अनुमोदन किया. दुर्भाग्य से 2017 में दिवंगत हुए जान अपनी इस पुस्तक को अपने जीवित रहते प्रकाशित नहीं देख पाए. कविताएं कालक्रम से नियोजित हैं और कोलाज उनके चाक्षुष (प्रत्यक्ष प्रमाण) और विषयगत प्रतिबिंदुओं के रूप में- पुकार और उत्तर के रूपक में. इसी पुस्तक में प्रकाशित एक इंटरव्यू में जान ने बताया है कि शायद कोलाज बनाना उन्होंने बीस बरस का होने से पहले शुरू कर दिया था.
कोलाज अपने मूल में एक तरह का खिलवाड़ होते हैं. उनमें कई आकार, कई आकृतियां, कई अभिप्राय, कई बिंब, कई छवियां अकस्मात जुड़ जाती हैं, बिना किसी स्पष्ट तर्क या संगति के. पर इस स्वेच्छाचारी ढंग से जुड़कर भी कोलाज सार्थकता प्राप्त कर लेते हैं. हर अर्थ विस्मयकारी होता है. कवि-चित्रकार ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा अर्थ निकल आएगा. वह दर्शक के लिए ही नहीं रचयिता के लिए भी विस्मय होता है. यों अगर हम ध्यान दें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तरह के तरह के कोलाजों से घिरे हैं. उन्हें किसी ने रचा नहीं है- वे स्वयंभू हैं. अपने आप किसी के चाहे बिना बन गये संयोग, जो हर समय विचित्र होते हैं. हम भले न कहें या न पहचानें- हमारा यथार्थ दरअसल अतियथार्थ है.
जान एशबरी के कोलाज कई तरह के हैं. सांप-सीढ़ी के खेल जैसे से लेकर कई तरह की कतरनों, पोस्टरों, पुराने चित्रों और फ़ोटोग्राफ़ों आदि का इस्तेमाल करते हुए चित्रित. उनसे जीवन की अपार चित्रमयता और बहुलता का एक आह्लादकारी रूप उभरता है. कविताओं की रेंज भी बहुत व्यापक है. उसमें लोकप्रिय गानों की पंक्तियों का भी प्रयोग है. जो गली-कूचों में फैला हुआ है उसे ग्रहण कर एक कविजनोचित जगह और परिष्कार देना जान को बखूबी आता है. वे भाषा और जीवन के बीच जो अनिवार्य दूरी और विभाजन है उसे पाट देते हैं.
भाषा और परिष्कार
इन दिनों भाषा की बात कोई नहीं करता जबकि उसका भयावह अवमूल्यन हो रहा है.
परिष्कार तो वैसे भी एक अस्पृश्य अवधारणा है जिसके होने या न होने को लेकर कोई चिंतित नहीं होता. अख़बारों, इलेक्ट्रानिक मीडिया और, दुर्भाग्य से, साहित्य तक की भाषा सिरे से भदेस होती जा रही है और हम सब हिंदी को एक विश्व भाषा मनवाने का एक निराधार और असंभव सपना देख रहे हैं. हिंदी चिंदी-चिंदी और गंदी हो रही है और हम प्रसन्न हैं कि वह फैल रही है. हिंदी भाषा की परंपरा की समझ और विरासत घट रही है पर हमें इसकी परवाह नहीं. हिंदी में ऐसी भयावह और व्यापक स्मृतिहीनता पहले कभी नहीं हुई और हम इसका एहतराम करने से भी कतरा रहे हैं.
हर नयी संवेदना भाषा का विस्तार करती है. उसके स्मृतिकोष में कुछ जोड़ती है. आज बेबाकी के नाम पर, संकोचहीनता के दावे के साथ जो भदेस हो रहा है उससे किसी तरह का जुड़ाव नहीं माना जा सकता. भदेस सिर्फ़ रुचि का नहीं दृष्टि का मामला है. आज उससे बार-बार आत्मरति टपक रही है यह अकारण नहीं हो सकता. अपने को केंद्र में मानना या हाशिये पर समझना लेखक के सामने यही दो विकल्प नहीं होते. अक्सर अच्छा लेखक हाशिये से केंद्र की ओर बढ़ता है और वापस हाशिये पर लौट जाता है. कभी-कभार ‘अहं ब्रह्मस्मि’ के भाव से प्रेरित होना उचित हो सकता है पर उसी भाव पर विजड़ित हो जाना सृजनविरोधी है. भाषा की मर्यादा सच्चाई की मर्यादा है, उसकी माप है. जितनी भाषा में अंट पाती है उतनी ही सच्चाई हमारे पल्ले पड़ती है. इसे लेखक से अधिक कौन जानता है? इसी का आभास इन दिनों कम मिलता है. हमारी भाषा में इसलिए सच्चाई पर पकड़ कमज़ोर पड़ रही है.
साहित्य भाषा में अभिव्यक्ति भर नहीं उसका परिष्कार भी होता है. कबीर ने सधुक्कड़ी का, तुलसीदास ने अवधी का, सूरदास ने ब्रज का, निराला-अज्ञेय-प्रेमचंद-रामचंद्र शुक्ल आदि ने खड़ी बोली का परिष्कार किया है. उन्होंने भाषा की सीमाओं का विस्तार किया, उसमें सचाई-दृष्टि -विचार-भाव आदि की संपदा में इज़ाफ़ा किया. इन सभी को भाषा की परवाह थी. वह उनके लिए निरा माध्यम भर नहीं थी- वह अनुभव का हिस्सा और उसका विस्तार-परिष्कार थी. अपने एक परिचित मुहावरे में कहूं तो वे भाषा को वहां ले गये जहां वह पहले नहीं गयी थी. यह जाना भी भाषा का परिष्करण है. इसे कुलीनता, आभिजात्य आदि कहकर लांछित करने से इसकी सच्चाई बदल नहीं जाती. साहित्य भाषा का परिष्कार है- सच्चा क्रांतिकारी साहित्य इसका अपवाद नहीं है. आजकल शिल्प के प्रति जो लापरवाही व्याप्त है और हर तरह के अख़बारीपन की कविता में घुसपैठ हो रही है वे इस परिष्कार के अभाव के लक्षण हैं. कोई भी भाषा सूक्ष्मता, जटिलता और परिष्कार को सहेजे बिना महान तो क्या आधुनिक समर्थ भाषा होने का दावा नहीं कर सकती. यह ख़तरे की घंटी है जिसे मैं अपने बूढ़े हाथों से बजा रहा हूं. कोई सुनता है?
–अशोक वाजपेयी
(साभार : सत्याग्रह. कॉम)